
Latest Version
December 16, 2023
Chaukhamba Surbharati Prakashan
Karmakanda
5.82 MB
1,000
Free
Report a Problem
More About मण्डप कुण्ड सिद्धि - Mandap Kunda Siddhi [PDF] Free PDF Download
मण्डप कुण्ड सिद्धि - Mandap Kunda Siddhi [PDF]
इस विश्व में ईश्वर के द्वारा निरन्तर यज्ञ चलता रहता है। वह इसमें मनुष्यों को भी निमित्त बनाता है। यज्ञ को क्रतु, अध्वर, होम, हवन, सवन आदि कहते हैं। प्राचीन काल में जब इस पृथ्वी पर चक्रवर्ती नरेशों का शासन था तब इस समस्त विश्व में यज्ञ- कार्य चलते रहते थे।
भारतीय ऋषि-मुनि भारत से बाहर दूर-दूर तक जाकर धर्मोपदेश देते थे तथा धार्मिक क्रियायें सम्पन्न कराते थे। कण्वगोत्रीय एक ऋषि ने महाभारत-युद्ध के कुछ काल पश्चात् ही अजपति देश (Egypt) में जाकर धर्म-प्रचार किया था। उन्हें ही मिश्रर्षि भी कहा जाता है।
भविष्यपुराण के अनुसार-
वासं कृत्वा ददौ ज्ञानं मिश्रदेशे मुनिर्गतः । सर्वान्म्लेच्छान् मोहयित्वा कृत्वा तानथ द्विजन्मनः ।।
ये मिश्रर्षि शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद - दोनों के मिश्रण से यागादि सम्पन्न कराते थे। उस समय ईजिप्ट (अजपति) में सूर्य की पूजा होती थी। मिश्र के प्राचीन शेख इन्हीं मिश्रर्षि के शिष्य थे। उस देश का नाम पश्चाद्वर्ती समय में 'मिश्र ऋषि' के नाम पर ही 'मिश्र' हो गया। ईसाइयत के प्रचार-प्रसार के पहले ग्रीक तथा रोम की जनता के साथ ही यूरोप के अनेक भूभागों में निवास करने वाली प्रजा भी हवन करती थी।
वहाँ उस समय धातु से निर्मित हवनकुण्डों का प्रचलन था; जिन्हें बाद में केवल 'हवन' कहा जाने लगा। वर्तमान समय में अंग्रेजी में प्रचलित ओवन (Oven) शब्द, जो कि एक प्रकार के अग्नि उपकरण के लिये प्रयुक्त होता है, प्राचीन हवन शब्द का ही अपभ्रंश है। 'आक्सफोर्ड आंग्ल शब्दकोश' इसका उद्गम 'जार्मनिक' भाषा से तथा चेम्बर का आंग्ल शब्दकोश प्राचीन ऐंग्लो सेक्शन भाषा से मानते हैं; परन्तु वास्तव में यह संस्कृत के मूल शब्द 'हवन' का ही अपभ्रंश है; क्योंकि महाभारत काल तक संस्कृत ही विश्वभाषा थी।
ईश्वरीय कार्य-यज्ञकार्य ईश्वरीय कार्य है; जिसमें ईश्वर ही यज्ञकर्त्ता है और वही हुतभुक् भी है। क्रतु का अर्थ 'ईश्वर' ही है-
करोति नित्यं सवनं जनानां करोति नित्यं मरणं जनानाम्।नित्यक्रियं विश्वमिदं समस्तं सर्गान्तमन्वेष्यति विष्णुगर्भम्।।
हविर्हि विष्णुः स जुहोति नित्यं क्रियाविधौ विश्वमिदं प्रगच्छन्। स एव होता स हि वास्तुहुत्यो बिभर्ति रूपाणि यतः स एकः ।। लोकेऽस्ति विष्णुर्हतभुक् प्रसिद्धः सूर्योऽग्निरापः पृथिवी मरुच्च। स्तोत्रा प्रदत्तानि हवींषि सद्यो भोक्तृस्वरूपे परियन्ति तानि ।।
विष्णुर्हि लोके हुतभुक्प्रसिद्धः सोऽग्निः स वा यज्ञसमिद्धतेजाः । वैश्वानरो वास्ति स वास्ति सूयों दावानलो वा स हि वाडवो वा ।।
यज्ञाङ्ग तथा उपाङ्ग-यज्ञ को सम्पन्न कराने के लिये उसके अङ्गों (मण्डप तथा कुण्डादि) की सम्यक् जानकारी आवश्यक है। वैदिक सूत्रग्रन्थों, ब्राह्मणग्रन्थों, पुराणों तथा तान्त्रिक ग्रन्थों में इन अङ्गों की विस्तृत विवेचना की गयी है।
इस विषय पर स्वतन्त्र साहित्य भी प्रचुर प्रमाण में लिखा गया है, जिसका लोप विदेशी एवं विधर्मी आक्रान्ताओं के आक्रमण से तथा कालक्रम से भी बहुत कुछ हो चुका है; परन्तु इतने पर भी जो कुछ उपलब्ध है, वह चमत्कृत करने वाला है; क्योंकि उसमें मण्डप तथा कुण्ड के उपाङ्गों (खात, नाभि, कण्ठ, मेखला तथा योनि एवं तोरण आदि) का सुस्पष्ट वर्णन मिलता है। दस हाथ या कुछ न्यून से लेकर एक सौ बीस या इससे भी अधिक लम्बे-चौड़े मण्डपों की निर्माण-विधि इन ग्रन्थों में मिलती है। उनमें भूमि के विभाग, स्तम्भों की सङ्ख्या तथा वलिका-काष्ठों की सङ्ख्या का भी उल्लेख है। पुराण में सत्ताईस प्रकार के मण्डपों की जानकारी मिलती है। ये मण्डप आकृतिभेद तथा आयामभेद से विपुल होते हैं।
कुण्डों के भेद-
कुण्डों के मुख्य दो भेद हैं- आयामभेद तथा आकृतिभेद। आयामभेद से कुण्ड एकहस्तात्मक, द्विहस्तात्मक, चतुर्हस्तात्मक, षड्हस्तात्मक, अष्ट- हस्तात्मक तथा दंशहस्तात्मक - इस तरह पाँच प्रकार के होते हैं। दूसरे प्रकार के भेद में मण्डप की आकृतियों के अनुसार भेद होते हैं। आकृति के अनुसार कुण्ड तीन प्रकार के होते हैं
१. कोणात्मक कुण्ड-
इनमें त्रिकोण कुण्ड, चतुरस्त्र कुण्ड, पञ्चास्त्र कुण्ड, षडस्र कुण्ड, सप्तास्त्र कुण्ड, अष्टास्त्र कुण्ड, नवात्र कुण्ड, रुद्र कुण्ड (एकादशास्त्र कुण्ड), षट्त्रिंशास्त्र कुण्ड एवं अष्टचत्वारिंशात्र कुण्ड होते हैं।
२. वर्तुल कुण्ड-
इनमें वृत्त कुण्ड, अर्धचन्द्र कुण्ड तथा पद्म कुण्ड होते हैं। सूर्य कुण्ड भी वर्तुलाकार होता है।
३. विशिष्ट कुण्ड-
इनमें योनि कुण्ड, असि कुण्ड, कुन्त कुण्ड, चाप कुण्ड, मुद्गर कुण्ड, शनि कुण्ड, राहु कुण्ड, केतु कुण्ड, चन्द्र कुण्ड, गुरु कुण्ड, भौम कुण्ड, बुध कुण्ड, शुक्र कुण्ड आदि होते हैं; जिनका वर्णन तान्त्रिक ग्रन्थों में मिलता है।
मण्डपकुण्डसिद्धि-
इस ग्रन्थ का नाम मण्डपकुण्डसिद्धि है; परन्तु कुछ लोग इसे 'कुण्डमण्डपसिद्धि' भी कहते हैं। ग्रन्थकार ने इसका नाम 'मण्डपकुण्डसिद्धि' ही रक्खा है। इस ग्रन्थ में सारे कुण्डों को चतुरस्रमूलक मानकर चतुरस्त्र, योनि कुण्ड, अर्धचन्द्र कुण्ड, त्रिकोए, कुट, वृत्त कुण्ड, षडस्न कुण्ड, पद्म कुण्ड तथा अष्टास्त्र कुण्ड-इन आठ आकारों वाले एक हाथ क्षेत्रफल से लेकर दस हाथ क्षेत्रफल तक के कुण्डों की रचना-विधि का सरलतापूर्वक वर्णन किया है।
इस ग्रन्थ के प्रथम अध्याय में तीस श्लोक हैं, जिनमें मण्डप निर्माण की विधि माप के सहित बताई गयी है। द्वितीय अध्याय में अट्ठारह श्लोक हैं, जिनमें माप-सहित कुण्ड-निर्माण की प्रक्रिया वर्णित है।
तृतीय अध्याय के दश श्लोकों में कुण्डों के उपाङ्गों -नाभि, खात, मेखला, योनि, कण्ठ आदि का मापसहित वर्णन है। इस प्रकार कुल अट्ठावन श्लोकों में इस ग्रन्थ में कुण्डनिर्माणसम्बन्धी साङ्गोपाङ्ग जानकारी दी गयी है; जिसके अनुसार कुण्ड की रचना तथा मण्डप-निर्माण एक सरल कार्य हो जाता है।
अन्यकार का परिचय-इस ग्रन्थ का निर्माण पवित्र कृष्णात्रि गोत्र में उत्पन्न श्री बूव शर्मा के पुत्र श्रीमद् विट्ठलदीक्षित ने किया है। यह बात स्वयं ग्रन्थकार ने प्रारम्भ के द्वितीय श्लोक में कही है।
उन्होंने इस ग्रन्थ की रचना श्री काशी जी के पुण्यनगर में शाके १५४१ में फाल्गुन शुक्ल द्वादशी, रविवार को आर्द्रा नक्षत्र में भगवान् विश्वनाथ की प्रसन्नता के लिये की है। यह बात ग्रन्थकार ने ग्रन्थ के अन्तिम श्लोक में स्वीकार की है। इस प्रकार इस ग्रन्थ का निर्माण विक्रम संवत् १६७६ तदनुसार सन् १६२० ईस्वी में हुआ था।
श्री विठ्ठलदीक्षित का जन्म शकाब्द १५०९ (संवत् १६४२ विक्रमी, सन् १५८५ ईस्वी) में हुआ था। इस प्रकार ग्रन्थकार ने पैतीस वर्ष की वय में ही इस ग्रन्थ की रचना की थी। ये फलित ज्योतिष के भी अच्छे विद्वान् थे। इन्होंने मुहूर्तकल्पद्रुम नामक ग्रन्थ की रचना भी की थी। इसके साथ ही इस पर इन्होंने 'मञ्जरी' नामक टीका भी लिखी थी। यह ग्रन्थ तथा इसकी टीका भी काशी में ही लिखी गयी थी। यह टीका चालीस वर्ष की आयु में लिखी गयी थी। टीका के अन्तिम श्लोक में इन्होंने लिखा है-
नन्दाम्बुतिथ्युन्मितशाककाले काशीपुरे विट्ठलदीक्षितेन । मुहूर्तकल्पद्रुममञ्जरीयं समर्पिता श्रीशिवपादपद्ये ।।
मण्डपकुण्डसिद्धि में जो दूसरा श्लोक है, वही प्रथम तीन चरणों में ज्यों का त्यों तथा चतुर्थ चरण में 'मुहूर्तकल्पद्रुम एष चक्रे' लिखकर मुहूर्तकल्पद्रुम ग्रन्थ की समाप्ति में दिया है। वहीं पर ग्रन्थकार ने अपनी कृति की प्रशंसा करते हुए तथा श्रीपतिरचित रत्नमाला को हीन बताते हुए लिखा है-
कल्पद्रुमश्चेत् किमु रत्नमाला चिन्तामणिं कर्करमेव मन्ये। यदेकदेशे किल मञ्जरीयं सारं विचारं कुरु तत्त्ववेदिन् ।।
इस श्लोक में जिस प्रकार से उन्होंने विद्वानों को सार-विचार करके स्वयं की कृति को अपनाने के लिये कहा है, उसी प्रकार मण्डपकुण्डसिद्धि की समाप्ति में भी इनका कथन है-
इति मण्डपकुण्डसिद्धिमेनां रुचिरां विट्ठलदीक्षितो व्यधत्त। अधिकाशिनगर्युमेशतुष्ट्यै विबुधः शोधयतादिमां विचार्य ।।
मण्डपकुण्डसिद्धि की किसी-किसी प्रति में एक निम्न श्लोक भी प्राप्त होता है,
जिसमें अपनी कृति की श्रेष्ठता का कारण भी ग्रन्थकार ने स्वयं ही बताया है-
अङ्गीकार्या मत्कृतिर्निर्मलेयं कस्मादेवं पण्डितान् प्रार्थयेहम्।।
इस प्रकार मण्डपकुण्डसिद्धि चतुष्कोण के आधार पर सभी कुण्डों का निर्माण करने वाला एक अनुपम ग्रन्थ है।
चैत्र शुक्ल एकादशी संवत् २०६१ विक्रमी
विदुषामनुचरः महर्षि अभय कात्यायन
Rate the PDF
User Reviews
Popular PDFs

![सूर्य पञ्चाङ २०८१ - Surya Panchanga 2081 (Nepali Patro) [PDF]](https://upayogibooks.com/images/1707273528.webp)
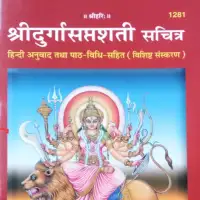
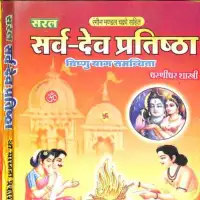


![वृहत् कर्मकाण्ड पद्धति - Vrihat Karmakanda Paddhati [PDF]](https://upayogibooks.com/images/1716396149.webp)
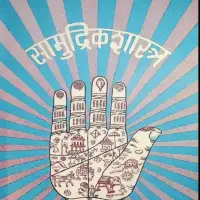
![दुर्गा सप्तसती हवन विधि - Durga saptasati havana vidhi [PDF]](https://upayogibooks.com/images/1702836557.webp)
![दीपावली पूजन विधि - Dipawali pujan vidhi [PDF]](https://upayogibooks.com/images/1699733648.webp)
Editor's Choice


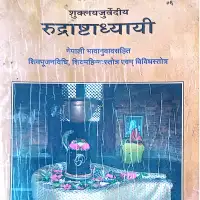


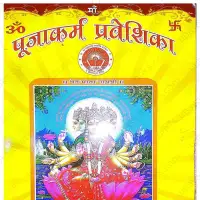
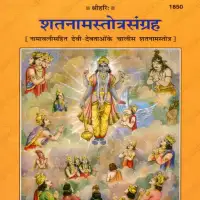
![गरुडपुराण सारोद्धार - Garuda Purana saroddhar Gita Press [PDF]](https://upayogibooks.com/images/1721869076.webp)
![साङ्ग सप्ताह मण्डप पुजा विधि - Sanga Saptaha Mandapa Puja Vidhi [PDF]](https://upayogibooks.com/images/1716489738.webp)
![अर्थ पञ्चक नेपाली भाषानुवाद - Artha Panchaka Nepali Translation [PDF]](https://upayogibooks.com/images/1716398011.webp)

![मण्डप कुण्ड सिद्धि - Mandap Kunda Siddhi [PDF]](https://upayogibooks.com/images/1702732334.webp)




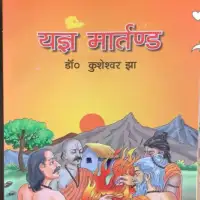
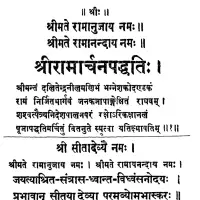
![श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पुजा विधि - Shri krishna janmashtami pujavidhi [PDF]](https://upayogibooks.com/images/1721811326.webp)
![मङ्गलचौथी पूजाविधि - Mangalchauthi Pujavidhi [PDF]](https://upayogibooks.com/images/1716655580.webp)
![चौरासीपूजाविधि - Chaurashi Puja Vidhi [PDF]](https://upayogibooks.com/images/1716655185.webp)
![ऋषितर्पणी पुजाविधि - Rishi Tarpani Puja Vidhi [PDF]](https://upayogibooks.com/images/1716654728.webp)
![श्रीवैकुण्ठ चन्द्रिका - ShriVaikuntha Chandrika [PDF]](https://upayogibooks.com/images/1716397488.webp)